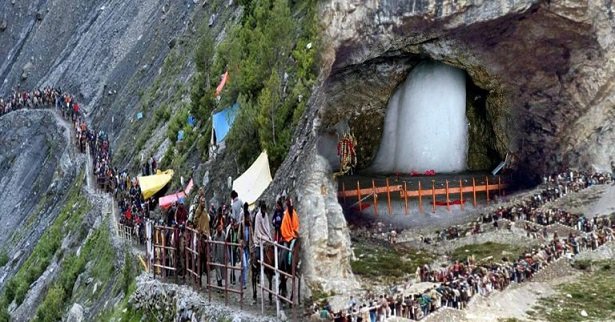निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक आधिकार है। इसलिए इससे छेड़छाड़ की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने राइट टु प्रिवेसी के मुद्दे पर छह फैसले लिखे, लेकिन गुरुवार को कोर्ट में सभी फैसलों का एक सारांश पढ़ा गया।
कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की धारा 21 का हिस्सा है। यह धारा भारत के नागरिकों के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है।
भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकारों की छह व्यापक श्रेणियों के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है जो न्यायोचित और न्यायालय में वाद योग्य हैं।
आइए जानते हैं कि वे छह मौलिक अधिकार कौन से हैंः-
1- स्वतंत्रता का अधिकार-
स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को बोलने, कहीं भी रहने, संघ या यूनियन बनाने और व्यापार करने का अधिकार देता है। जो कि अनुच्छेद (१९-२२) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
2- शोषण के विरुद्ध अधिकार-
शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद (2३-२४) के अंतर्गत आता है, जो बालश्रम के विरोध में और मानव तस्करी रोकने का अधिकार देता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से भी रोकता है।
3- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार- ‘
अनुच्छेद (२५-२८) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित हैं। धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार धर्म को मानने, उसका आचरण और प्रचार करने की अनुमति देता है। सिक्खों को कटार रखने की अनुमति भी देता है। वहीं धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता के साथ ही स्कूल-कॉलेज में धर्म की उपासना करने का मौलिक अधिकार भी देता है।
4- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार-
अनुच्छेद (२९-३0) के अंतर्गत प्राप्त संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार हमे अपनी संस्कृति और भाषा को बचाए रखने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने और स्कूल-कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उसके संचालन का अधिकारी भी देता है।
5- संपत्ति का अधिकार-
संपत्ति का मौलिक अधिकार नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद (३१) के अनुसार प्रावधान किया गया है।
6- संवैधानिक उपचारों का अधिकार-
डॉ॰ भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद ३२-३५) को ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ की संज्ञा दी थी। सांवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर ५ प्रकार के प्रावधान हैं-
१- बन्दी प्रत्यक्षीकरण : बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ़्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ़्तारी का तरीका या कारण ग़ैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
२- परमादेश : यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
३- निषेधाज्ञा : जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुक़दमें की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ‘निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख’ जारी करती हैं।
४- अधिकार पृच्छा : जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब न्यायालय ‘अधिकार पृच्छा आदेश’ जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
५- उत्प्रेषण रिट : जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।